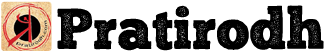आस्था नहीं, अन्वेषण पर आधारित हो इतिहास
May 26, 2014 | Pratirodh Bureau
भारतीय इतिहासलेखन के विकास, असहमति की परंपरा तथा बौद्धिक अभिव्यक्तियों को बाधित करने के मौजूदा प्रयासों पर रोमिला थापर की कुलदीप कुमार से बातचीत. (अनुवाद: अभिषेक श्रीवास्तव)
आपकी पुस्तक दि पास्ट बिफोर अस आरंभिक उत्तर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर विस्तार से बात करती है. जानकर अचरज होता है कि आखिर क्यों और कैसे इस विचार की स्वीकार्यता बन सकी कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव है.
ये जो मेरी पुस्तक छह माह पहले प्रकाशित हुई है, आरंभिक उत्तर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर केंद्रित है. जिसे मैं आरंभिक उत्तर भारत कहती हूं, उसका आशय ईसा पूर्व 1000 से लेकर 1300 ईसवीं तक है. यह पुस्तक अनिवार्यत: इतिहासलेखन का एक अध्ययन है और इतिहास के लेखन का यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने भारत में, खासकर प्राक्-आधुनिक भारत के संदर्भ में बहुत ध्यान नहीं दिया है. आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ तो इसका खासा महत्व पहचाना जाना शुरू हो चुका है लेकिन प्राक्-आधुनिक इतिहास के संदर्भ में ऐसा कम है. यह इसलिए अहम है क्योंकि यह उस दौर के इतिहासकारों और विचारधाराओं का अध्ययन है, जो इतिहास के लेखन की ज़मीन तैयार करते हैं. इस लिहाज़ से यह इतिहास दरअसल इतिहासलेखन पर एक टिप्पणी है.
हर कोई यह कहता पाया जाता था कि भारतीय सभ्यता में इतिहासबोध का अभाव है. मुझे आश्चर्य होता कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है. मैंने इसी सवाल से अपनी शुरुआत की. मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जटिल सभ्यता आखिर क्यों अपने अतीत के प्रति एक बोध विकसित क्यों नहीं कर सकी और विशिष्ट तरीकों से अतीत से क्यों नहीं जुड़ सकी. आखिर को हर समाज की अपने अतीत के प्रति एक समझ रही है और अपने लेखन के विभिन्न माध्यमों में समाजों ने अपने अतीत को उकेरा है.
फिर, यह क्यों कहा गया कि भारतीय सभ्यता में इतिहासबोध का अभाव था? मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक लेखन से इसका लेना-देना होना चाहिए.
आपका आशय प्राच्यवादियों से है?
मेरा आशय आंशिक तौर पर प्राच्यवादियों से और बाकी प्रशासक इतिहासकारों से है, जैसा कि उन्हें अकसर कहा जाता है. वे अंग्रेज प्रशासक थे जिन्होंने इतिहास भी लिखा, जिसका एक अहम उदाहरण विन्सेन्ट स्मिथ हैं. लेकिन इससे पहले भी 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय इतिहास को एक ऐसे इतिहास के रूप में देखा जाता था जो एक स्थिर समाज से ताल्लुक रखता था, जिसमें कुछ भी बदला नहीं था. इससे एक तर्क यह निकलता था कि यदि कोई समाज बदलता नहीं है, तो जाहिर तौर पर इतिहास का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है क्योंकि इतिहास तो बदलावों का दस्तावेजीकरण होता है, बदलावों की व्याख्या होता है. तो यदि आप किसी समाज को स्थिर कह देते हैं, तो उसमें इतिहासबोध के नहीं होने की बात कह कर आप एक हद तक सही जा रहे होते हैं.
स्थिर की बात किस अर्थ में है?
स्थिर का मतलब ये कि कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ ही नहीं और समाज की संरचना जैसी थी वैसी ही बनी रही. फिर उन्होंने काल की अवधारणा के साथ इस तर्क को नत्थी कर डाला और कहा कि काल की प्राचीन भारतीय अवधारणा चक्रीय थी. यानी निरंतर एक ही चक्र खुद को दुहराता रहा, जो कि तकनीकी तौर पर सही नहीं है क्योंकि आप काल की चक्रीय अवधारणा का अध्ययन करें तो साफ़ तौर पर पाएंगे कि चक्र का आकार बदलता रहता है और प्रत्येक चक्र में धर्म की मौजूद मात्रा भी परिवर्तनीय होती है.
बल्कि, वास्तव में घटती ही है…
हां, घटती है. इसीलिए यह आवश्यक है कि कोई न कोई सामाजिक बदलाव ज़रूर हुआ हो जिसने यह परिवर्तन पैदा किया हो. लेकिन ऐसा नहीं माना गया. हालांकि इसके पीछे सबसे अहम कारक यह तथ्य था कि एक औपनिवेशिक संरचना, एक औपनिवेशिक प्रशासन उस समाज के लोगों के ऊपर उपनिवेश या उपनिवेशित समाज की अपनी समझ को थोपना चाहता है. इसलिए, ऐसा करने का एक बढि़या तरीका यह कह देना है कि: ”आपके लिए आपके इतिहास का अन्वेषण हम करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कैसा था.” और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने बिल्कुल यही काम मोटे तौर पर किया जिसके लिए उसने प्राक्-आधुनिक भारतीय इतिहास के सार के रूप में दो धार्मिक समुदायों की उपस्थिति को समझा.
यानी हिंदू और मुसलमान?
हां,,. और इसका सिरा जेम्स मिल के कालावधीकरण (हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल) तक और इन दो धार्मिक समुदायों के संदर्भ में भारतीय समाज को देखने की एक विशुद्ध सनक तक खिंचा चला जाता है.
महाभारत को पारंपरिक तौर पर इतिहास की श्रेणी में रखा गया था. अतीत को देखने का भारतीय तरीका क्या बिल्कुल ही भिन्न था?
आरंभिक भारत के ग्रंथों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसे पाठ संभव हैं जो इतिहास के कुछ आयामों को प्रतिबिंबित करते हों. ब्रिटिश उपनिवेशवाद की दलील थी कि इकलौता ग्रंथ जो इतिहास को प्रतिबिंबित करता था वह 12वीं सदी में कश्मीर के कल्हण का लिखा राजतरंगिणी था. उनका कहना था कि यह एक अपवाद था. हालांकि करीब से देखने पर कुछ दिलचस्प आयाम खुलते नज़र आते हैं. मसलन, कुछ ग्रंथों को इतिहास के रूप में वर्णित किया गया है. इस शब्द का अर्थ वह नहीं था जो आज की तारी में हम ‘इतिहास’ से समझते हैं. इसका ससीधा सा अर्थ था कि ‘अतीत में ऐसा हुआ रहा.’ आप ‘इतिहास पुराण’ शब्द को अगर लें, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खयाल से अतीत में ऐसा ही हुआ रहा होगा. लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण यह है कि एक चेतना है जो इतिहास सदृश है, भले ही वह ऐतिहासिक रूप से सटीक ना हो. मेरी दिलचस्पी इसी में है.
मैंने अपनी पुस्तक में यही तर्क दिया है कि इस प्रश्न के तीन पहलू हैं जिनकी पड़ताल की जानी है. पहला, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक चेतना को दर्शाते हैं, जिन्हें हमें ऐतिहासिक रूप से सटीक लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये उन लोगों का अंदाजा दे पाते हैं जो इस दिशा में कुछ हद तक सोच रहे थे. फिर उस ऐतिहासिक परंपरा की बात आती है जिसका मैंने जि़क्र किया है, जहां अतीत के संबंध में यथासंभव उपलब्ध तथ्य, आख्यान और सामग्री को सायास जुटाकर समूची सामग्री को एक शक्ल देने का प्रयास है. अपने तर्क के लिए मैंने विष्णु पुराण को लिया है जहां यह सब उपलब्ध है, जो अतीत को आख्यान के तौर पर वर्णित करता है- जिसकी शुरुआत मिथकीय मनु से होती है, फिर उसके वंशज समूहों, वंशावलियों, मध्यकाल में उपजे कुटुम्बों और अंतत: राजवंशों और उनके शासकों का वर्णन है. आधुनिक इतिहासकार के लिए जो बात अहम है, वह अनिवार्यत: ऐतिहासिकता का प्रश्न नहीं है- कि कौन से पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं- बल्कि यह कि प्रस्तुत आख्यान दो भिन्न किस्म के समाज-रूपों और ऐतिहासिक बदलाव को दिखाता है या नहीं.
आपका आशय इश्वाकु से है?
हां, कुछ इश्वाकु के वंशज और कुछ इला के. दरअसल, यह राजवंशों से अलहदा एक कौटुम्बिक समाज का रूप है.
इसके बाद, यानी गुप्तकाल के बाद, इसके रूप बदलते हैं और आख्यानों का लेखन सचेतन ढंग से और स्पष्टता के साथ किया जाता है जिनमें दावा है कि ये वास्तविक रूप से घटी घटनाओं के आख्यान हैं. दिलचस्प है कि इसमें बौद्ध और जैन आख्यान सम्मिलित हैं. बौद्ध और जैन परंपराओं में इतिहासबोध बहुत तीक्ष्ण था तो संभवत: इसलिए कि इनके विचार और शिक्षाएं ऐसे ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित थे जो वास्तव में हुए थे. इतिहास में बड़ी स्पष्टता से उनकी निशानदेही की जा सकती है. दूसरी ओर, उत्तर-पौराणिक ब्राह्मणवादी परंपरा तीन किस्म के लेखन का गवाह रही है जो वर्तमान और अतीत का दस्तावेज हैं और इसीलिए इतिहास लेखन में सहायक है. पहली श्रेणी राजाओं की जीवनकथा है, जिसे ‘चरित’ साहित्य कहते हैं- हर्षचरित और रामचरित और ऐसे ही ग्रंथ. दूसरी श्रेणी उन शिलालेखों की है जो तकरीबन हर राजा ने बनवाए. कुछ शिलालेख बहुत ही लम्बे हैं. उनमें राजवंशों के इतिहास और राजाओं की गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है. यदि कालानुक्रम से किसी एक राजवंश के सभी शिलालेखों को एक साथ रखकर आदि से अंत तक पढ़ा जाए, तो परिणाम के तौर पर हमें राजवंश का इतिहास मिल जाएगा. गुप्तकाल के बाद के दौर में क्या हुआ था- कम से कम कालानुक्रम और राजवंशों के संदर्भ में- उस पर हमारा आज का अधिकतर मौजूद अध्ययन मोटे तौर पर इन्हीं शिलालेखों पर आधारित है. हाल ही में इन शिलालेखों से हमें भू-संबंध, श्रम और सत्ताक्रम के राजनीतिक अर्थशास्त्र में आए बदलावों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं.
यहां तक कि अशोक की राजाज्ञाओं में भी एक इतिहासबोध दिखता है, जो उन्होंने अपनी प्रजा को निर्देश पर तत्काल अमल करने के लिए जारी किए थे हालांकि उसके दिमाग में अपनी भावी पीढ़ी का भी ध्यान तो रहा ही होगा.
हां, बेशक ऐसा ही है. कुछ में तो वह यहां तक कहता है कि उसे आशा है कि उसके पुत्र और पौत्र हिंसा को त्याग देंगे और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो भी दंड सुनाते समय दया बरतेंगे. यानी, भावी पीढि़यों के लिए दस्तावेज का एक बोध तो था ही और मुझे लगता है कि शिलालेखों में यह विशेष तौर से ज़ाहिर है. आखिर किसी पत्थर पर या ताम्बे की प्लेट पर या फिर विशेष तौर से निर्मित किसी शिला अथवा मंदिर की दीवार पर खुदवाने का इतना कष्ट उन्होंने क्यों उठाया? इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बाद की कई पीढि़यां भी उसे पढ़ती रहें.
तीसरे किस्म का लेखन ज़ाहिर तौर से कालक्रमानुसार लिखे गए अभिलेख थे. राजतरंगिणी कश्मीर का एक इतिवृत्त है जो कि उच्च कोटि का साहित्य है. कुछ बहुत छोटे-छोटे इतिवृत्त भी हैं जिन्हें संजो कर रखा गया, हालांकि वे कल्हण जैसे उत्कृष्ट नहीं हैं.
मध्यकाल में राजदरबारों में कालक्रमानुसार अभिलेखों का लिखा जाना जारी रहा और रामायण व महाभारत जैसे महाग्रंथों के नए संस्करण आए तथा बाद में नई भाषाओं में भी इन्हें लिखा गया.
आप दोनों महाग्रंथों रामायण और महाभारत को कैसे देखती हैं? हिंदू सामान्य तौर पर सोचते हैं कि इनमें जो कुछ लिखा है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ घटा था. हस्तिनापुर और अयोध्या में तो इन महाग्रंथों की ऐतिहासिकता को जांचने के लिए खुदाई भी हुई थी.
भारतीय महाग्रंथों को लेकर एक इतिहासकार के समक्ष दो समस्याएं होती हैं. कुछ मायनों में तो ये भारत के संदर्भ में विशिष्ट हैं क्योंकि और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां के महाग्रंथ अनिवार्यत: धर्मग्रंथ बन गए हों. वहां वे प्राचीन नायकों का वर्णन करने वाले काव्य हैं जबकि यहां वे पवित्र ग्रंथ बन गए हैं. इसलिए हमारे सामने दो समस्याएं हैं. एक तो बेहद बुनियादी समस्या जो रह-रह कर अकसर उभर आती है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा मज़बूती से हमारे सामने उपस्थित होगी. ये वह फ़र्क है, जो हमें आस्था और इतिहास के बीच बरतना होता है. यदि एक इतिहासकार के तौर पर आप महाभारत को पढ़ रहे हैं, तो यह मान लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पवित्र साहित्य मान रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है. एक इतिहासकार के तौर पर आप समाज के संदर्भ में उसके पाठ को बरत रहे हैं तथा सेकुलर और तर्कवादी तरीके से बस उसका विश्लेषण कर रहे हैं.
इससे दिक्कत पैदा होती है क्योंकि एक आस्थावान व्यक्ति के लिए ये वास्तविक घटनाएं हैं और यही वे लोग हैं जो वास्तव में पढ़ाते रहे हैं, जबकि एक इतिहासकार के लिए मुख्य सरोकार की चीज़ यह नहीं है कि ग्रंथ में वर्णित व्यक्ति और घटनाएं ऐतिहासिक हैं या नहीं. सरोकार इस बात से है कि ये ग्रंथ जो वर्णन कर रहे हैं, उसका व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और व्यापक समाज के साहित्य के तौर पर इनकी भूमिका क्या है. हमारे पास कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं है कि ये लोग थे. जब तक हमें साक्ष्य नहीं मिल जाते, इस पर हम कोई फैसला नहीं दे सकते. ये दो बिल्कुल अलहदा क्षेत्र हैं लेकिन आज हो ये रहा है कि आस्था के छोर से बोल रहे लोगों- सब नहीं, एक छोटा सा हिस्सा- में एक प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि वे मांग कर रहे हैं कि इतिहासकार उसे ही इतिहास मान ले जिसे आस्थावान लोग इतिहास मानते हैं. एक इतिहासकार ऐसा नहीं कर सकता. आज इतिहास को आस्था पर नहीं, आलोचनात्मक अन्वेषण पर आधारित होना होगा.
यही वजह है कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव की मांग की जा रही है.
हां, बेशक. इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि एनसीआरटी की जिन पाठ्यपुस्तकों पर यह बहस चल रही है- जिन्हें हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तक सब खंगाल कर लिखा था- उनकी आलोचना और उनमें बदलाव की मांग धार्मिक संस्थानों और ससंगठनों की ओर से आ रही है. दूसरे इतिहासकार ऐसी मांग नहीं कर रहे. यह इस बात का एक अहम संकेत है कि कैसे आस्था, एक मायने में, इतिहास के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है.
दूसरे, हमें एक सवाल पूछना होगा: क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर जिसे आस्था बताया जा रहा है उसमें कोई राजनीतिक तत्व भी है? क्योंकि जो संगठन ऐसी मांग उठाते हैं, उनके राजनीतिक संपर्क ज़रूर हैं. चाहे जो भी हो, व्यापक अर्थों में ‘राजनीतिक’ शब्द का प्रयोग करें तो समाज में वर्चस्वशाली स्वर वाला कोई भी संगठन राजनीतिक प्रवृत्ति से युक्त होगा ही. इसलिए, इतिहास में आस्था का अतिक्रमण सिर्फ धर्म और इतिहास की टकराहट नहीं है. यह एक खास तरह की राजनीति के साथ भी टकराना है.
इन दिनों ऐसा लगता है कि हर किसी की धार्मिक भावनाएं इतनी नाज़ुक हैं कि तुरंत आहत हो जाती हैं. क्या हमारे यहां असहमति की परंपरा रही है?
बेशक हमारे यहां असहमति की परंपरा रही है. जब कभी पुराने लोगों ने, खासकर बाहरी लोगों ने भारत में धर्म के बारे में लिखा, उन्होंने अकसर यहां के दो अहम धर्म समूहों का हवाला दिया- ब्राह्मण और श्रमण. चाहे वह ईसा पूर्व चौथी सदी में मेगस्थनीज़ रहे हों या 12वीं ईसवीं में अल-बरूनी, ये सभी ब्राह्मण और श्रमण की बात करते हैं, जैसा कि सम्राट अशोक ने पंथों का जि़क्र करते हुए अपने शिलालेखों में भी इन पर बात की है.
तो क्या यह वैदिक और गैर-वैदिक का फ़र्क है?
इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि अल-बरूनी तक पहुंचने के क्रम में आप ऐसे ब्राह्मणों को पाएंगे जो उस वक्त वेद और पुराण दोनों की शिक्षा दे रहे थे. पुराणों पर आधारित हिंदू धर्म कहीं ज्यादा लोकप्रिय था, जैसा कि चित्रकला, शिल्पकला और कुछ साहित्य श्रेणियों में दिखाई देता है. श्रमण में बौद्ध और जैन आते थे, जिन्हें ब्राह्मण नास्तिक कहते थे. यह संभव है कि इस श्रेणी के भीतर ऐसे पंथ भी रहे हों जो वेदों पर आस्था नहीं रखते थे, मसलन भक्तिमार्गी शिक्षक. इस द्विभाजन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पतंजलि ने अपने संस्कृत व्याकरण में दोनों को परस्पर विरोधी बताया है और इनकी तुलना सांप व नेवले से की है. इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणवादी परंपरा से पर्याप्त और खासी असहमतियां मौजूद थीं.
तो क्या यह किसी संघर्ष का रूप ले सकी?
हां, कुछ मामलों में ऐसा हुआ. राजतरंगिणी में कल्हण बताते हैं कि किसी कालखंड में- पहली सदी के मध्य के आसपास- बौद्ध भिक्षुओं पर हमले हुए और उनके विहारों को नष्ट किया गया था. फिर, तमिल स्रोतों से पता चलता है कि जैनियों को सूली पर चढ़ाया गया. शिलालेखों में शैव और जैनियों तथा शैव और बौद्धों के बीच अंतर का जि़क्र है. भले ही असहिष्णुता से जुड़ी घटनाओं का जि़क्र यहां मिलता है लेकिन कोई जिहाद या धर्मयुद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी.
इसकी वजह बेशक यह हो सकती है कि प्राक्-आधुनिक भारतीय सभ्यता में भेदभाव का स्वरूप उतना धार्मिक प्रकृति का नहीं था बल्कि यह था कि जाति संरचना का हिस्सा रहे लोगों ने जाति संरचना से बाहर रहे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया होगा. यह भारत में हर धर्म के साथ देखा जा सकता है, चाहे वह यहां का रहा हो या बाहर से आया रहा हो.
असहमति इस अर्थ में एक दिलचस्प स्वरूप धारण कर लेती है कि ब्राह्मणवादी और श्रमणवादी दोनों ही परंपराओं के भीतर भी असहमत लोग थे. विमर्श और विवाद की तयशुदा प्रक्रियाओं में इसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है. पहले, विरोधी विचार को संपूर्ण और तटस्थ तरीके से सामने रखा जाता है, फिर वादी विस्तार से उसके अंतर्विरोधों को उजागर करता है, आखिर में या तो सहमति होती है अथवा असहमति.
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि असहमति को मान्यता दी जाती है और उस पर बहस की जाती है. तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां विभिन्न शासकों के दरबार में हुई किसी बहस में किसी व्यक्ति के जीतने या हारने का संदर्भ आता है.
और क्या पूर्वपक्ष यानी प्रतिवादी का विचार ईमानदारी से सामने रखा जाता था?
हां, क्योंकि यह वाद-विवाद एक सार्वजनिक आयोजन होता था.
क्या लेखन में भी ऐसा ही था?
हां, लेखन में भी यही स्थिति थी. जैसा कि हर अच्छा अध्येता करता है, यदि आप किसी चीज़ की निंदा करना चाहते हों तो सबसे पहले आपको उसे गहराई से समझना होगा अन्यथा आपकी निंदा सतही करार दी जाएगी. विद्वता का सार यही है और ऐसा उस वक्त होता था. असहमति से निपटने का एक अन्य तरीका, जिसे प्रभावकारी माना जाता था, वो यह था कि ब्राह्मणवादी परंपरा असहमत व्यक्ति की सहज उपेक्षा कर देती थी. ब्राह्मणों और बौद्ध व जैन के बीच के तनाव बड़े दिलचस्प तरीके से विष्णु पुराण में उकेरे गए हैं जिसमें बौद्धों और जैनियों को ”महामोह” की संज्ञा दी गई है- यानी बहकाने वाले लोग. कहानी यह थी कि इन लोगों ने ब्रह्माण्ड के बारे में समझाने के लिए एक सिद्धांत गढ़ा था जो कि दरअसल बहकावा था जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता था. इसलिए, बहकावेबाज़ होने के लिए इनकी निंदा की गई है. असहमति से निपटने का यह एक अन्य तरीका था.
सामान्यत: यह कहा जाता है कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी. मैं इस दलील को नहीं मान पाती क्योंकि उन्होंने बौद्धों के कुछ विचारों को भी हथिया लिया था और इससे कहीं ज्यादा, बौद्ध धर्म के पतन के कई और कारण हैं. यह जानना दिलचस्प है कि मठ स्थापित करने का चलन, जो कि इस रूप में पहले नहीं मौजूद था, बौद्ध और जैन विहारों की संरचना के समरूप जान पड़ता है. इनका असर यह हुआ कि किसी शिक्षण को बड़े पैमाने पर आयोजित और प्रसारित करने के लिए उसके पीछे एक संस्थान का होना अनिवार्य है.
चाहे जो हो, शंकराचार्य को तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा ही जाता रहा.
हां, वे थे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने श्रमणवादी परंपरा से कुछ कारक आंदोलन को संगठित करने के लिए उधार लिए और यह एक ऐसी बात है जिसे हम नहीं मानते हैं. विचारधारा का अन्वेषण करते वक्त यह जानना दिलचस्प होगा कि विरोधी परंपरा से क्या कुछ उधार लेकर हथियाया जा रहा है.
एकाधिक रामकथाओं पर आपका क्या विचार है? बौद्ध और जैन परंपराओं में तो इनके कई संस्करण हैं.
इन कहानियों के अपने कई संस्करण लोगों के पास थे. रामकथा पहले भी एक लोकप्रिय कथा थी और आज भी है. बौद्ध जातक कथाओं में आपको कहीं-कहीं इनके तत्व बिखरे हुए मिल जाएंगे. जिसे दशरथ जातक कहा जाता है, वह रामकथा का ही एक हिस्सा है. इसमें राम और सीता दोनों वनवास पर जाते हैं, वहां से लौटते हैं और मिलकर 16,000 साल तक राज करते हैं. बौद्ध संस्करण में एक अहम फ़र्क यह है कि यहां राम और सीता भाई-बहन हैं. इसका जैन संस्करण पउम चरिय (पद्म चरित) संपूर्णत: जैन लोकाचार से परिपूर्ण है. इसमें दशरथ, राम, सीता और अन्य सभी पात्र जैन हैं. साफ़ तौर पर यह एक बड़े नायक के चरित का सीधे-सीधे अपनी परंपरा में उठा लिया जाना है.
इस संस्करण में तो दशरथ जीवन के अंत में संन्यास ले लेता है…
हां, दशरथ संन्यास ले लेता है और सीता आश्रम में चली जाती है. उसका अंत नहीं होता, न ही उसे धरती निगल जाती है. दिलचस्प है कि पउम चरिय ऐतिहासिकता का दावा करता है और कहता है कि ये घटनाएं वास्तव में हुई थीं और वह बताता है कि बाकी सारे संस्करण गलत हैं और वही वास्तव में बता सकता है कि घटनाएं कैसे घटित हुई थीं. यानी यह दूसरे संस्करणों को चुनौती दे रहा है. यह एक ऐसा पाठ है जिसमें रावण और अन्य राक्षसों को मेघवाहन वंशावाली का सदस्य बताया गया है जिसका संबंध चेदियों से है, जिसका एक दिलचस्प समानांतर ऐतिहासिक संदर्भ हमें कलिंग के खरावेला के शिलालेखों में मिलता है जो खुद को मेघवाहन बताता है और चेदि का जि़क्र करता है. पउम चरिय का सबसे अहम तर्क यह है कि इन राक्षसों का कथा के दूसरे संस्करणों में दानवीकरण किया गया है. इसमें रावण के दस सिर नहीं हैं. वह दरअसल नौ विशाल रत्नों का एक हार पहनता है जिनमें प्रत्येक में उसका सिर दिखाई देता है. इसका प्रयास यह है कि वाल्मीकि रामायण और अन्य संस्करणों में मौजूद फंतासी के तत्वों की एक तार्किक व्याख्या की जाए.
इतने ढेर सारे रामायण क्यों मौजूद हैं? इसका लेना-देना दरअसल हिंदू धर्म की प्रकृति से है और एक इतिहासकार के तौर पर हिंदू धर्म के बारे में यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करती है. यह किसी एक ऐतिहासिक शिक्षक, एक पावन ग्रंथ, सामुदायिक पूजा, संप्रदाय और एक समान आस्था प्रणाली पर आधारित नहीं है, जैसा कि हम यहूदी-ईसाई परंपरा में पाते हैं. यह वास्तव में पंथों का एक जुटान है. आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ में आस्था रख सकते हैं, जब तक कि आप उसके कर्मकांडों को अपना रह हों. और ये कर्मकांड अकसर जाति आधारित होते हैं. आप किसी कर्मकांड को होता देखकर उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, चढ़ावे और प्रार्थना के आधार पर मोटे तौर से यह जान सकते हैं कि यह ब्राह्मणवादी है या गैर-ब्राह्मणवादी. इसलिए मेरे खयाल से संप्रदाय के संदर्भ में जाति बहुत अहम पहलू है और यदि कोई धर्म अनिवार्यत: कई संप्रदायों के सह-अस्तित्व व संसर्ग पर आधारित हो, तो ज़ाहिर तौर पर आस्था और कर्मकांडों के संस्करणों में भिन्नता तो होगी ही.
इसीलिए, कहानियां एकाधिक होंगी. और इसका उस सामाजिक संस्तर से पर्याप्त लेना-देना होगा जहां से उसका लेखक आ रहा है. मसलन, भारतीय प्रायद्वीप की कुछ लोक कथाओं में सीता युद्ध में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह करती है, जो कि इस बात का लक्षण है कि इस कहानी का महिलाओं का लिखा संस्करण उनका अपना है.
यह बात कहीं भी अैर किसी भी कहानी के साथ सही हो सकती है. आप देखिए कि लातिन अमेरिका में ईसाइयत का क्या हश्र हुआ, कि वहां जिस-जिस क्षेत्र में वह गया, लोगों ने अपनी परंपराओं के हिसाब से उस कहानी को बदल डाला. यह वास्तव में किसी कथा की महान संवेदनात्मकता का द्योतक है कि कैसे वह लोगों की कल्पनाओं को अपने कब्ज़े में ले लेती है और लोग उसे अपने तरीके से ढाल लेते हैं.
आजकल बहुलतावाद और विविधता को लोग सहिष्णुता से नहीं लेते हैं. आपके विचार में एक जनतांत्रिक समाज के तौर पर भारत के विकास के साथ ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि हम इस मोड़ तक आ गए?
यहां एक बार फिर ऐसा लगेगा कि मैं उपनिवेशवादियों को आड़े हाथों ले रही हूं लेकिन इसका ज्यादातर लेना-देना 19वीं सदी के विचारों से है. औपनिवेशिक विद्वान और प्रशासक हिंदू धर्म को समझ नहीं पाए क्योंकि वह यहूदी या ईसाई धर्म के उनके अपने अनुभवों के सांचे में बैठ नहीं सका. इसलिए उन्होंने तमाम संप्रदायों को एकरैखिक परंपरा में बांधकर और इन्हें मिलाकर एक धर्म का आविष्कार कर डाला जिसे उन्होंने हिंदूइज़्म कहा. आस्थाओं और कर्मकांडों का अपना एक इतिहास था लेकिन एकल ढांचे में इनकी समरूपता बैठाने का विचार नया था. इनमें से कुछ घटक तो बहुत पहले से विद्यमान थे. मसलन, शक्त-शक्ति की परंपरा यानी तांत्रिक परंपरा सातवीं और आठवीं सदी के स्रोतों में ज्यादा मज़बूती से उभर कर आई थी. फिर भी, हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच इसका विचार और कर्मकांड काफी पहले से मौजूद रहा हो. सामान्यत: लोग मानते हैं कि यह शायद अवैदिक लोगों और निचली जातियों व ऐसे ही लोगों का धर्म था.
शिल्पकला इत्यादि में इनकी अभिव्यक्ति खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों तक कैसे पहुंच गई?
जिस तरह समाज और उसका इतिहास बदलता है, वैसे ही अभिजात वर्ग के घटकों में भी बदलाव आता है. हम सभी इस विचर को सुनते-समझते बड़े हुए हैं कि जाति एक जमी हुई निरपेक्ष चीज़ है. अब हालांकि हम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक दायरे कहीं ज्यादा खुले हुए थे. सही परिस्थितियां हासिल होने पर जातियों के भीतर के समूह उच्च पायदान तक खुद को पहुंचाने के दांव भी खेलते थे.
और इसी के लिए वे वंशावलियां बनवाते थे…
हां, ठीक बात है. एक व्यक्ति या एक परिवार सत्ता और वर्चस्व की स्थिति तक पहुंच कर भी उन देवताओं की पूजा कर सकता है जो पुराणों का हिस्सा नहीं हैं, जैसे कि कुछ देवियां. लेकिन, चूंकि अब उन्हें न अभिजात तबके ने अपना बना लिया है इसलिए उन देवताओं को उस देवसमूह में डाला जा सकता है और वह पौराणिक हिंदू धर्म का हिस्सा बन जाता है. यही बात है कि पुराणों का अध्ययन जितना रोमांचकारी है उतना ही ज्यादा जटिल भी है क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी चीज़ कहां से आ रही है. ऐतिहासिक नज़रिये से देखें, तो ये तमाम तत्व कहां फल-फूल रहे थे और कब व कैसे वे मुख्यधारा के धर्म का हिस्सा बना दिए गए, इसका पता लगाना बड़ा दिलचस्प काम हो सकता है.
जब मैंने 19वीं सदी के उपनिवेशवादियों का जिक्र किया तो मेरी कोशिश उस एकल धर्म यानी हिंदू धर्म के निर्माण की तरफ ध्यान आकृष्ट करने की थी जिसके कुछ विशिष्ट और परिभाषित कारक हैं. राजनीति जब धर्म के स्वरूप और उसकी अंतर्वस्तु को तय करने लग जाती है, तो वहां साम्प्रदायिकता की परिघटना का प्रवेश हो जाता है. मुस्लिम साम्प्रदायिकता के साथ ऐसा करना आसान है क्योंकि इस धर्म का बाकायदे एक इतिहास है जिसमें उसका एक संस्थापक है और उसकी शिक्षाएं इत्यादि हैं. इसी के साथ हिंदू साम्प्रदायिकता समानांतर आकार ले लेती है. दोनों प्रतिरूप हैं. इसमें हिंदू धर्म को इस तरीके से दोबारा सूत्रीकृत किया जाना है जिससे लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करने में धर्म का इस्तेमाल संभव हो सके. यही वजह है कि ऐतिहासिकता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो उठता है. यदि आपने तय कर दिया कि वह राम है जिसने धर्म की संस्थापना की थी, तब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वह बुद्ध, ईसा और मोहम्मद की तरह ही ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में था. इन तीनों के बारे में तो कोई विवाद नहीं है. अशोक ने लुम्बिनी में एक लाट लगवाई थी जिस पर लिखा था कि यहां बुद्ध जन्मे थे. रोमन इतिहासकारों ने ईसा के बारे में और अरब के इतिहासकारों से मोहम्मद के बारे में लिखा ही है.
यानी, एक ऐतिहासिक संस्थापक और एक पवित्र ग्रंथ तो होना ही है. बंगाल में जब पहली बार अदालतें अस्तित्व में आईं, तो न्यायाधीशों पे पंडितों से पूछा कि वे किस पुस्तक की वे कसम खाएंगे. उनकी बाइबिल या कुरान कौन सी किताब है? कुछ ने रामायण का नाम लिया, कुछ लोगों ने उपनिषद और कुछ अन्य ने गीता का नाम लिया. यह विवाद अब भी बना हुआ है. गांधीजी ने गीता को बड़ा महत्व दिया था, तो बहुत से लोगों को लगने लगा कि यही पवित्र ग्रंथ है. इसकी जरूरत ही नहीं है. वह कई पवित्र किताबों में एक थी. इसी तरह अगर आप राम को भगवान मानते हैं, तो वह तमाम भगवानों में एक भगवान, तमाम अवतारों में एक अवतार था.
अब सवाल आता है कि एक संगठन तो होना ही चाहिए. यदि धर्म कई सम्प्रदायों से मिलकर बना है, तो इन्हें साथ कैसे लाया जाए? एक तरह से देखें तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ऐसे ही संगठन धर्म को संगठित करने का एक आरंभिक प्रयास थे ताकि समूचे समुदाय की ओर से उक्त संगठन बोल सके. ऐसा हो नहीं सका. 1920 और 1930 के दशक में इन प्रयासों के विफल हो जाने के बाद हिंदू धर्म की औपनिवेशिक समझ के आधार पर हिंदुत्व का उभार हुआ और हिंदू धर्म के भीतर से ही एक ऐसे धर्म को निर्मित करने की कोशिश की गई जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. अब, इसके लिए क्या ज़रूरी था? इसके लिए हिंदू को ही यहां का मूलनिवासी परिभाषित करने की ज़रूरत थी क्योंकि उसका धर्म की ब्रिटिश भारत की चौहद्दी के भीतर पनपा था. यानी बाकी सब बाहरी हुए. यानी धर्म अब नागरिकता का अधिकार या बाहरी की परिभाषा को तय कर रहा था. यह बात राजनीतिक रूप से बेहद अहम है. यह एक बड़ा संक्रमण है जो कि पूरी तरह 19वीं सदी के विचार पर आधारित है- औपनिवेशिक और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय, दोनों ही विचार.
यानी कि वेंडी डोनिगर ”दि हिंदूज़: ऐन आल्टरनेटिव हिस्ट्री” जैसी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने या वापस लेने की मांग राजनीतिक है.
पेंग्विन से प्रकाशित यह पुस्तक उन बहुलताओं पर चर्चा करती है जिनसे मिलकर हिंदू धर्म बना है. यह विभिन्न सामाजिक सम्प्रदायों और धर्म के उनके स्वरूप के बारे में है जो उन्होंने हिंदू विचार और प्रार्थना पद्धति के मूल से लिया था और हिंदू धर्म के निर्माण में इस आधार पर जो योगदान दिया था. एक ऐसी पुस्तक जो वैकल्पिक पंथों और बहुलतावाद पर चर्चा करती हो, उसे प्रसारित किए जाने को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि वह विकल्पों और बहुलताओं के बीच फल-फूल नहीं सकती है. उन्होंने इस मसले को खुले तौर पर नहीं उठाया क्योंकि राजनीतिक रूप से यह दुरुस्त कदम नहीं होता. इसीलिए उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, मसलन कि डोनिगर कैसे कह सकती हैं कि राम ऐतिहासिक पात्र नहीं थे. विद्वानों में अधिकांश का मत है कि अगर यह गलत नहीं है तो यह सुनिश्चित भी नहीं है.
फिर उनके ऊपर शिव की व्याख्या में फ्रायडीय विश्लेषण प्रयोग करने का आरोप लगा और उनके लिखे कुछ वाक्यों पर आपत्ति जताई गई. हर किसी को आपत्ति करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि वह क्यों गलत है और उसकी वजहें गिनवानी होंगी. आप यह नहीं कह सकते कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. यह पुस्तक एक प्रस्थापना को सामने रखती है. आपको इसका प्रतिवाद पेश करना होगा. प्रस्थापना का प्रतिवाद प्रस्तुत करना ही प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुकूल होगा. लेकिन दुर्भाग्यवश, ”आहत भावनाओं” के आधार पर किताबों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाले अधिकतर लोग वे हैं जिनके पास प्रतिवाद करने की क्षमता नहीं है.
एक भावना यह भी है कि तमाम लोग इतिहास पर ऐसी लोकप्रिय पुस्तकें लिख रहे हैं जो तथ्यात्मक रूप से बहुत सही नहीं हो सकती हैं. मसलन, चार्ल्स एलेन की ‘अशोक’.
देखिए, इतिहस हमेशा से दो बीमारियों से ग्रस्त रहा है. एक तो, जैसा कि एरिक हॉब्सबॉम ने बहुत सटीक सुझाया था, कि इतिहास राष्ट्रवाद के लिए अफ़ीम जैसा है. अतीत और भविष्य की सारी भव्य निर्मितियां इतिहास पर खड़ी होती हैं. इसलिए, इतिहास ने राष्ट्रवाद में, और इसी वजह से राजनीति में, बहुत अहम योगदान दिया है. आप उससे बच नहीं सकते.
दूसरे, चूंकि किन्हीं तरीकों से इतिहास को महज एक आख्यान माना गया है- जो कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नृशास्त्र और अन्य विधाओं के साथ नहीं है, जिनकी अपनी एक प्रविधि है. लोग मानकर चलते हैं कि कोई भी शख्स जिसने इतिहास पर छह किताबें पढ़ ली हैं वह सातवीं किताब लिखने के योग्य है. लेकिन हम ललोग जो कि इतिहास के क्षेत्र में ही काम करते हैं, लगातार कहते रहे हैं कि इतिहास में विश्लेषण की अपनी एक प्रविधि होती है. इसके स्रोतों के साथ तमाम किस्म के तकनीकी पहलू जुड़े होते हैं. यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है. यह दूसरी बीमारी है जिससे इतिहास ग्रस्त है और ग्रस्त रहेगा.
हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों के बीच भी एक विभाजन है. एक तरफ पेशेवर तौर पर प्रशिक्षित इतिहासकार हैं जो ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रविधियों से परिचित हैं. दूसरी तरफ वे नौसिखिये हैं जो छह किताबें पढ़कर सातवीं लिख देते हैं.
एक अनुशीलन के तौर पर आज की तारीख में इतिहास, 50 साल पहले की तुलना में कहां खड़ा है?
पिछले पचास साल में इतिहास भारी बदलावों से गुज़रा है जिसका अंदाज़ा औसत और सामान्य पाठकों को शायद बिल्कुल नहीं है. उनकी इतिहास की अवधारणा बीसवीं सदी से पहले की बनी हुई है. विभिन्न प्रवासी समूहों के साथ यही दिक्कत है कि वे इतिहास को उन धारणाओं के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं जिनसे वे 50 साल पीछे से परिचित रहे हैं. वे लगातार अगली पीढि़यों तक इसे दुहराते रहते हैं जबकि हम उन धारणाओं से काफी दूर चले आए हैं. यही वजह है कि हमारे बीच इतना कम संवाद है.
मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में साठ के दशक की शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, तो हमारे बीच इस बात को लेकर काफी बहसें, बैठकें, परिचर्चाएं होती थीं कि इतिहास के पाठ्यक्रम को राजनीतिक और राजवंशीय इतिहास से विस्तारित कर सामाजिक और आर्थिक इतिहास तक ले जाने की ज़रूरत है. बहसें काफी गरम भी हो जाती थीं और लोग पूछते थे कि यह सामाजिक और आर्थिक इतिहास नाम की नई चिडि़या कौन सी है. आज कोई यह सवाल नहीं पूछता. इसमें कुछ भी नया नहीं है. इसके बाद हम तमाम दूसरी दिशाओं में दूसरी चीज़ों की ओर बढ़े. एक लंबा दौर इतिहास के मार्क्सवादी लेखन का रहा. फिर, जिसे ”लिटरेरी टर्न” कहा गया, उसमें लोगों की काफी दिलचस्पी रही, यानी एक सांस्कृतिक मोड़ से युक्त उत्तर-औपनिवेशिकतावाद. तब इतिहासकारों ने पाठ की ओर रुख किया और उनका दोबारा अन्वेषण शुरू किया.
उत्तर-आधुनिकतावाद का क्या हुआ?
उत्तर-आधुनिकतावाद भी आया है. यह एक बिल्कुल नए किस्म का दायरा है जिसमें हम जैसे कुछ लोग बहुत सशक्त पक्ष रखते हैं. लेकिन सवाल यह है कि आपको उन बौद्धिक बदलावों को लेकर सचेत रहना होगा जो इधर बीच आए हैं. मैं नहीं चाहती कि मुझे दंभी समझा जाय, लेकिन यह बात मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि आज ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां जो लोग भी समाज विज्ञान में लेखन का काम कर रहे हैं, वे ऐसा एक ठस बौद्धिक पक्ष लेकर कर रहे हैं. उनका काफी अध्ययन रहा है, उन्होंने सैद्धांतिकी गढ़ी है, उन्होंने अतीत को समझने की कोशिश की है, लेकिन उनके सामने जो अड़चन है वह बेहद बुनियादी पक्ष से आती है. इसीलिए, कोई बहस करना ही बहुत मुश्किल जान पड़ता है क्योंकि आज अच्छे इतिहासकार जिस आधारभूमि पर सैद्धांतिकी गढ़ रहे हैं, उसे एक औसत पाठक शायद ही समझ पाता है और जो नहीं पढ़ते उनकी तो यह बेहद कम समझ में आता है. और जो लोग किताबें प्रतिबंधित करने या वापस लेने जैसी मांग उठाते हैं, वे तो उन किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं.
(साभार: गवरनेंस नाउ, 6 मई 2014) Link: http://www.governancenow.com/news/regular-story/making-sense-past-and-present-romila-thapar