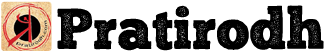मुझे तुम्हारे इस यक़ीन पे शक है
Oct 9, 2014 | Panini Anandइस फ़िल्म में कश्मीर केवल वैसे ही है जैसे खादी चोरों की बैठक में गांधी का चित्र. इस्तेमाल करो और किनारे लगाओ. जो लोग इस फ़िल्म के आधार पर निर्देशक या उनके उस्ताद के बारे में कोई बड़ी राय बना रहे हैं, मेरे खयाल से वे लोग रेत में पानी खोद रहे हैं.

पर्दे पर कश्मीर पहले भी आया. सुंदर और हतप्रभ करता हुआ. सुलगता और झकझोरता हुआ. इसबार भी दिखा एक अंतराल के बाद और सुंदर लगा. कैमरा ही नहीं, संवाद, अभिनय, मेक-अप, सेट, रंग, लय सबकुछ बेहतरीन. संगीत भी अच्छा. बिल्मिल-बिल्मिल सबसे बेहतरीन गीत रहा हालांकि उससे कश्मीर से ज़्यादा शेक्सपियर झांक रहा था. ठीक वैसे ही जैसे ‘सात ख़ून माफ़’ में रेड आर्मी की धुन की नकल पर ‘डारलिंग आंखों से आंखें चार करने दो’ को भारतीय कानों तक ऊतार दिया जाता है. नकल तो नकल है लेकिन अच्छी हो तो बुरी बात भी नहीं है. अच्छा यह लगा कि इस गीत पर सेट, संगीत और नृत्य संयोजन कमाल का था और रंगों से लेकर प्रस्तुति तक लगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभिमंच में बैठे हैं, सिनेमाघर में नहीं. यह सबकुछ ठीक था अगर अंग्रेज़ी साहित्य की शास्त्रीयता की मार खाए निर्देशक ने सिर्फ़ सिनेमा बनाया होता. सिनेमा बनाया, बनाइए. बेचना है, बेचिए. लेकिन उम्मीद मत बेचिए. दर्द मत बेचिए. आंसू मत बेचिए. ख़ून मत बेचिए… कश्मीर मत बेचिए जनाब. सिनेमा बेचिए. बस.
बेचने वाले डेविड धवन भर होते या होते सूरज बड़जात्या तो हम मान लेते कि भई, तीन घंटे का कीर्तन कॉकटेल है, देखिए और मनोरंजन करके सो जाइए. इस दुखिया संसार में तीन घंटे कोई हंसा सके, हल्का महसूस करा सके, यह कम नहीं है. देखिए और आगे बढ़िए. लेकिन साहेब, यहाँ बेचनेवाला शातिर है. वो बाज़ार के उन कलंदरों का शागिर्द है जो पहले माचिस और हूतूतूतू बेच चुके हैं. जिन्हें मालूम है कि घाव और आंसुओं पर कैसे उगाए जा सकते हैं शैवाल और फिर उनसे मुनाफ़ा कमाया जा सकता है. बोलचाल की भाषा में ये लोग इसे व्यवसायिक मजबूरी और बाज़ार का दबाव जैसे विशेषणों से नवाजते हैं. गुलज़ार विद्यालय क्या पंजाब को केवल उतना भर जानता है जितना कि माचिस में उन्होंने दिखाया. या फिर उतना भर ही है आमजन के विद्रोहों का सच जितना कि हूतूतूतू में दिखता है. बिना सरोकार का पैरोकार वैसा ही होता है जैसा कि शहर का बनिया जो आदिवासी बस्तियों में जड़ीबूटियों, पेड़ों के गोंद और महुए के तेल के बदले शकर के गट्टे और तरबूज तौल आता है. गुलज़ार और उनके गुरुकुल का महान सिनेमाबोध और सिनेमा के प्रति योगदान इसी प्ले सेफ़ येट आउटस्टेंडिंग के सिद्दांत पर आधारित है.
बेचैनियों के बीच कुछ साथी बोले कि भई सिनेमा है, सिनेमा की तरह देखिए. हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो लोग इसे कश्मीर में एक सिनेमा के तौर पर देख रहे हैं, देखें. लेकिन जो इसे कश्मीर पर एक सिनेमा समझने की भूल कर रहे हैं, वो ऐसा न करें. इस फ़िल्म में कश्मीर केवल वैसे ही है जैसे खादी चोरों की बैठक में गांधी का चित्र. इस्तेमाल करो और किनारे लगाओ. जो लोग इस फ़िल्म के आधार पर निर्देशक या उनके उस्ताद के बारे में कोई बड़ी राय बना रहे हैं या मान चुके हैं कि कश्मीर को अगर कोई आवाज़ देकर पुकार रहा है तो वह विशाल हृदय यह ही है, मेरे खयाल से वे लोग रेत में पानी खोद रहे हैं. जो रोना-धोना कश्मीर के नाम पर इस फ़िल्म के इर्द-गिर्द फैलाया गया है, वो कश्मीर की पीठ पर बैठकर इसे हर संभावित दर्शक तक पहुंचाने का मार्केटिंग मंत्र है. कश्मीर इस फ़िल्म के साथ घिसटता हुआ चला आ रहा है. इस आस में कि शायद इसी बहाने मेरी भी कोई बात तो उठेगी, मेरा भी कोई दर्द सुनेगा. मेरे अंदर भी कोई झांकेगा. लेकिन झांकेगा तब जब अंदर कश्मीर होगा. बाहर से रूमानी और रूहानियत के रंगों से रंगे कश्मीर के पर्दे जब खुलते हैं तो सामने होता है केवल शेक्सपियर और दो भाइयों के बीच एक औरत… नफ़रत, वहशत, बदला. कश्मीर का काम खत्म हुआ. वो बाहर खूंटे से बंधा हुआ है. देखिए और मज़ा लीजिए.
हैदर कश्मीर के दशकों लंबे सवाल पर अपनी टाप की ठोकरें मारकर शोर पैदा करती एक कहानी है जिसका ताना-बाना चचा-भतीजे का संघर्ष है. जिसमें एक पत्नी, प्रेमिका, पति, भाई, बेटा, पुलिसिया, मुखबिर, मददगार और हत्यारा, सबकुछ एक ही मजहब और इलाके के हैं. बाहर से सिर्फ़ हवाएं आती हैं. इन हवाओं में बहकने वाला, बहकाने वाला, बहकाव के खिलाफ़ बोलने वाला, हर कोई वहीं का है. वहीं खड़ा है या गड़ा है. हैदर गाली दे रहा है एएफ़एसपीए को लेकिन उसे बदला लेना है चाचा से. रूहदार अलगाववादी है लेकिन किसी के घर के पचड़े में सारा ज़ोर दिए है. जो एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे हैं, वो बच नहीं रहे, न मार रहे हैं. वे सब इंतज़ार कर रहे हैं. यह बात हिलाल मीर के सामने कही गई थी कि बदले से सिर्फ़ बदला पैदा होता है लेकिन हिलाल मरकर ख़्वाबों में भी बदले की रट लगाए है. गज़ाला को बदला किसी से नहीं लेना लेकिन आखिर वो सबसे बदला ले लेती है. अपने दूसरे पति से, बेटे से, समाज से और खुद से भी. अर्शी और उसके भाई इसलिए मार दिए गए हों जैसे ताकि कोई रोने वाला पीछे न छूटे. अधूरे परिवारों, आधी विधवाओं, इंतज़ार और अकेलेपन को जीते लोग कश्मीर का सच हैं लेकिन फ़िल्म को इससे क्या.
तो क्या केवल इसलिए इस फ़िल्म की तारीफ़ की जाए कि यह कश्मीर से जुड़ी है. कश्मीर से जुड़ने का मतलब क्या हैदर का कश्मीरी होना भर है. क्या वाकई हैदर की लड़ाई के सारे हत्यारे, साजिशकर्ता और मोहरे उस कब्रिस्तान में सदा के लिए सो चुके हैं. आपने कश्मीर दिखाया, नए ढंग से दिखाया, अच्छा लगा. विशिष्ट भी. तो, आगे क्या. इसका विषय से या कश्मीर के सवाल से क्या ताल्लुक. या हैदर की कहानी ही कश्मीर की कहानी है. क्यों सस्ते और छोटे उदाहरणों में समेटकर निपटाने की बेकली दिखाई देती है. यह सहज ही हो गया या सोच-समझ के ऐसा किया गया. क्या इसीलिए बड़े सवाल केवल छोटे संकेतों की तरह बड़ी चतुराई से पिरोए गए हैं इस कहानी में. ताकि आप सतरंगे दिखें. सबकी पसंद का कोई न कोई रंग तो मिल ही जाएगा सभी को.
फ़िल्म में कैमरा अच्छा न होता, स्क्रिप्ट में काव्यात्मकता न होती और आखिर तक सच के सच की तरह सामने आने की उम्मीद न होती तो पता नहीं कितनी देर केवल पोस्टर पर छपे बर्फ़ के गोले और फ़िरन हमें रोके रह पाते. सिनेमाघर में बारहां याद आई कांधार, टर्टेल्स कैन फ्लाई, सिटी ऑफ़ गॉड, अर्थ एंड ऐशेज़ और न जाने कितनी ही फ़िल्में जो अपने-अपने कश्मीर की कथाएं कह रही हैं. लगा कि हैदर तड़पकर अभी पर्दे से निकलेगा और ऐसी किसी फ़िल्म की रील में अपना कोना खोजकर फिर से बोलेगा- हम हैं कि हम नहीं. पर नहीं, हैदर कहीं नहीं जा सका. न जाएगा. क्योंकि हैदर मुंबई वाला है, कश्मीर वाला नहीं. यह फिल्म एक घूंट दूध- एक घूंट मट्ठा का असमंजस लिए हुए है. शुरुआत से आखिर तक.
…………………………………
फुट नोट्स- अब आमिर ख़ान क्या करेंगे. उनका रेडियो को शाहिद उठा ले गया. हैलो टेस्टिंग भी कर दिया. और तो और, शाहिद ने एक नहीं, दो-दो सलमान मार दिए. मने, ऐसे ही.