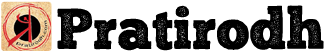भारतीय साहित्य और प्रगतिशील आंदोलन की विरासत
Dec 11, 2011 | गोपाल प्रधानपिछले साल हमने जिन कवियों की जन्मशती मनाई वे हैं शमशेर, नागार्जुन, फ़ैज़, केदारनाथ अग्रवाल आदि. आगामी वर्षों में रामविलास शर्मा तथा मुक्तिबोध की भी जन्मशतियाँ हम मनाने जा रहे हैं.
इन सबको जोड़कर देखें तो हिंदी उर्दू साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का पूरा खाका उभरकर सामने आता है. इस मुद्दे पर बात इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदी में न सिर्फ़ प्रगतिशील आंदोलन के समय बल्कि आज भी इस धारा के अवदान को नकारने की आदत मौजूद है.
सबसे पहले तो यह ध्यान दें कि यह आंदोलन अपने ठीक पीछे के साहित्यकारों की विरासत को ग्रहण करते हुए उसे आगे बढ़ाता है. इसी संदर्भ में हम रामविलास शर्मा द्वारा निराला तथा मुक्तिबोध द्वारा जयशंकर प्रसाद के मूल्यांकनों को समझ सकते हैं.
प्रेमचंद तो इसकी स्थापना से ही जुड़े हुए थे. निराला भी कहीं न कहीं इस नई प्रवृत्ति के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं.
आज भले ही दलित साहित्य के पैरोकार और तमाम लोग इन साहित्यकारों के साहित्य को सहानुभूति मात्र का साहित्य कहें लेकिन सच यही है कि यदि इन लोगों ने अपने जमाने में लड़ाई न लड़ी होती तो आज नए यथार्थ को पाँव नहीं मिलते.
प्रेमचंद को उनके साहित्य के कारण घृणा का प्रचारक कहा गया. निराला कुजात ही रह जाते अगर प्रगतिशील आलोचकों ने उनके साहित्य की मान्यताओं को स्थापित करने के लिए संघर्ष न किया होता.
प्रगतिशील आंदोलन की दीर्घजीविता पर परदा डालने के लिए उसे महज आठ साल चलनेवाला आंदोलन बताया गया. कहा गया कि ‘तार सप्तक’ के साथ प्रगतिशील आंदोलन खत्म हुआ. इस तरह 36 से 53 कुल इतना ही इसका समय है
यह भी भुला दिया गया कि जिस ‘तारसप्तक’ की वजह से उसे मरा घोषित करने का रिवाज चला उसमें राम विलास शर्मा भी एक कवि के बतौर शामिल थे जिनकी जन्मशती भी शुरू होने जा रही है. और तो और, नए कवियों के इस संग्रह को निकालने की योजना भी फ़ासीवाद विरोधी लेखक सम्मेलन में बनी थी जिसकी अध्यक्षता डांगे ने की थी.
इन तथ्यों पर परदा नासमझी में नहीं, जानबूझकर डाला गया ताकि इसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को छिपाया जा सके. यह काम प्रगतिवाद के विरोधियों ने तो किया ही, अनेक प्रगतिशीलों ने भी हवा का साथ देने के लोभ में इस अभियान पर मौन धारण किया.
इस साहित्य में विदेशी प्रभाव को, खासकर रूसी साहित्य की प्रेरणा, को चिन्हित करके जड़विहीन साबित करने की कोशिश की गई मानो संरचनावाद या अस्तित्ववाद की जड़ें भारत में थीं.
यह भी भुला दिया गया कि गांधीजी ने दक्षिण अफ़ीका में जिस आश्रम की स्थापना की थी उसका नाम प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार तोलस्तोय के नाम पर था. प्रेमचंद और रवीन्द्रनाथ ठाकुर यूँ ही रूस के प्रशंसक नहीं थे. उस समय रूस पूरी दुनिया में मनुष्यता के लिए लड़ने वाली शक्तियों की आशा का केंद्र था. प्रेमचंद ने अपने लेख ‘महाजनी सभ्यता’ में रूस को नई सभ्यता के उदय की भूमि माना.
प्रगतिशील धारा से सबसे बड़ी दिक्कत उन चिंतकों को थी जो साहित्य को किसी भी तरह जनता से जोड़ने के विरोधी थे. साहित्य के रूप संगठन को ही उसका प्राण समझने वालों की परंपरा बेहद मजबूत थी. इसके अवशेष आज भी मिलने मुश्किल नहीं हैं. साहित्य को महज पाठ बना देने के पीछे एक मकसद उसे मनुष्य से अलग कर देना भी है. संरचनावाद का अनुसरण करते हुए साहित्य की स्वायत्तता का नारा भी उसकी सर्व तंत्र स्वतंत्र दुनिया बसाने के लिए ही दिया गया था.
प्रगतिशील धारा के लेखकों पर सबसे बड़ा आरोप कला की उपेक्षा का लगाया गया लेकिन उनकी कला को आज फिर से समझने की जरूरत है. जैसे कोई सफल लोकप्रिय फ़िल्म बनाना फ़िल्म कला पर जबर्दस्त अधिकार की माँग करता है उसी तरह लोगों के कंठ में बसने वाले गीत लिखना भी बहुत बड़ी कला साधना की माँग करता है.
इस उद्देश्य के लिए प्रगतिशील कवियों ने समूचे साहित्य को खँगाला. शास्त्रीय छंद शास्त्र के साथ ही उन्होंने लोक कंठ में बसी धुनों को अपनाया. उन्होंने घोषित तो नहीं किया लेकिन उनकी आसान सी लगने वाली कविताओं के पीछे कितनी साधना है इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ही काफ़ी होगा. मुक्तिबोध कि कविता है ‘मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं’. इस कविता को उस छंद में लिखा गया है जो रावण के शिव स्तोत्र का छंद है. ध्यान देने की बात यह है कि जयशंकर प्रसाद ने भी इसी धुन पर ‘हिमाद्रि तुंग शृंग पर’ लिखा था.
हिंदी उर्दू का साझा
प्रगतिशील आंदोलन की जिस दूसरी विशेषता को रेखांकित करने की जरूरत है वह यह कि हिंदी उर्दू का अब तक का सबसे बड़ा साझा उसी दौरान निर्मित हुआ. यह कोई सर्व धर्म समभाव नहीं था बल्कि लोगों की जुबान में उनके लिए लिखने का आग्रह था.
आजादी के बाद जिस मध्य वर्ग को सत्ता हासिल हुई, उसकी पूरी कोशिश आम जनता से साहित्य को दूर रखने की थी. हालाँकि आज के घोटालेबाजों को देखते हुए उस समय का मध्यवर्ग आम जन ही लगता है लेकिन आजादी के बाद सत्ता की नजदीकी ने उसे खास होने का बोध करा दिया.
धीरे धीरे रेशमी भाषा में महीन कताई को ही मूल्यवान बताया जाने लगा और उसमें से मेहनत के पसीने की गंध को दूर करने की कोशिशें शुरू हुईं. लेकिन उस दौर में भी सामने आ रहे मध्य वर्ग की आदतों को मुक्तिबोध ने चिन्हित किया ‘चढ़ने की सीढ़ियाँ सर पर चढ़ी हैं’.
मुक्तिबोध को बेवजह उस जमाने में अज्ञेय का प्रतितोल नहीं समझा जाता था. अज्ञेय के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता जहाँ उसके द्वीप बनने में थी वहीं मुक्तिबोध के तईं ‘मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते’. आज तो भारतीय मध्यवर्ग में ‘ऊँचे से ऊँचे, और भी ऊँचे, उनसे भी ऊँचे’ पहुँच जाने की आकांक्षा ही उसकी पहचान बन गई है. मध्यवर्ग की जनता से बढ़ती दूरी ने हिंदी के कुछ बौद्धिकों पर घातक असर डाला है तभी तो हिंदी के एक बड़े लिक्खाड़ को किसान आंदोलन ब्लैक मेलिंग लग रहे हैं.
प्रगतिशील साहित्यिक परंपरा को पीछे धकेलने की कोशिशों को मार्क्सवाद को लगे धक्के से बड़ी ऊर्जा मिली थी. इसका वैचारिक नेतृत्व उत्तर आधुनिकता ने किया था. लेकिन अब पश्चिमी जगत में भी उत्तर आधुनिकता को भरोसेमंद और कारगर व्याख्या मानने में कठिनाई महसूस हो रही है. हालांकि हमारी हिंदी में अभी इसकी तरफ़दारी जारी है.
जैसे अमेरिकी रास्ते पर दुनिया भर में सवाल खड़ा होने के बावजूद भारतीय शासक उसके पिछलग्गूपन में ही अपनी मुक्ति देख रहे हैं वैसे ही भारतीय और हिंदी के कुछ पश्चिममुखी बौद्धिक अभी ‘मूँदहु आँख कतहुँ कछु नाहीं’ की अवस्था में हैं.
अमेरिकी साम्राज्यवाद की नंगई तथा उसके विरुद्ध दुनिया भर में खासकर लातिन अमेरिकी देशों में पैदा हुए आंदोलनों ने मार्क्सवाद को फिर से बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है. इस बहस में मार्क्सवाद की पुरानी मान्यताओं को दोबारा बदले हालात में जाँचा परखा जा रहा है. देर से ही सही इस माहौल का असर भारत के साथ साथ हिंदी पर भी पड़ना तय है लेकिन आलोचकों की नई पीढ़ी को भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा.
आलोचना की नई पीढ़ी
आलोचकों की एक नई फ़ौज ने हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर दस्तक देनी शुरू कर दी है. यह फ़ौज अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले राजनीतिक रूप से अधिक समझदार है. हालाँकि इस पर भी पाठ और पुनर्पाठ जैसी उत्तर आधुनिक शब्दावली का दबाव है और विचारधारा की छूत से अलग करके साहित्य की स्वायत्त दुनिया आबाद करने के शोरोगुल का असर भी है.
लेकिन इसके सामने चुनौती प्रगतिशील साहित्य की विरासत को उसी तरह आगे बढ़ाने की है और इस चुनौती का उत्तर भी उन्हें उसी तरह देना होगा जैसे प्रगतिशील आलोचकों ने साहित्य खासकर हिंदी साहित्य में जो कुछ भी मूल्यवान था उसे आयत्त करते हुए वैचारिक दबदबा हासिल किया था.
इनको परंपरा का उसी तरह नवीकरण करते हुए उसे प्रासंगिक बनाना होगा जैसे नागार्जुन, राम विलास शर्मा और मुक्तिबोध ने अपने समय में किया था.
प्रगतिशील आलोचना की विरासत महज रूपवाद के समक्ष समर्पण की नहीं है. इसकी मुख्यधारा फूहड़ समाजशास्त्र का आरोप झेलकर भी साहित्य को समाज के जरिए समझती रही है.
सौभाग्य से नए आलोचकों ने अपनी बहसों से इस वैचारिक क्षमता का अहसास भी कराया है. लेकिन उनके सामने कार्यभार कठिन है.
प्रगतिशील आंदोलन के दिनों के मुकाबले स्थितियाँ बदली हुई हैं. तब सोवियत रूस की शक्ल में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था और देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की निश्चिंतता थी. इस फ़र्क को तब के नौकरीपेशा और आज के असुरक्षित वेतनभोगियों की तुलना करके समझा जा सकता है.
आज उदारीकरण सिर्फ़ शब्द नहीं है बल्कि एक असुरक्षित जीवन पद्धति का नाम है. जिन सवालों के जवाब अंतिम माने जा रहे थे वे आज फिर से जिंदा हो गए हैं. इसीलिए नए आलोचकों को चौतरफ़ा चुनौती का हल खोजना है.
उन्हें थोड़ी जिद के साथ भी थोड़ा एकतरफ़ापन का आरोप झेलते हुए भी दोबारा साहित्य को उसकी सामाजिक जड़ों की तरफ़ खींच लाना होगा.