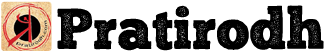सियासत का गुनाह और बेगुनाहों की सियासत
May 16, 2012 | राजीव यादवसवाल आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों का नहीं और न ही लोकतांत्रिक ढांचे के पुलिस तंत्र और निरंतर चलते रहने वाली न्यायिक प्रक्रिया का है. सवाल आतंकवाद के नाम पर संचालित उस पूरे ढांचे का है जो इसे एक समुदाय से जोड़कर कर तो देख ही रहा है पर साथ-साथ यह भी कोशिश कर रहा है कि यह पीडि़त, दोषी उनके एहसानों तले जीने को मजबूर हो.
आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को छोड़ने की सपा सरकार की बात ने एक बार फिर मुस्लिम समाज को लिटिमस टेस्ट के लिए तैयार कर दिया है. अगर वह छोड़े जाते हैं तो तुष्टीकरण का आरोप और नहीं तो एक बार फिर उन्हें वोटों की राजनीति द्वारा छला गया. दरअसल आतंकवाद के नाम पर निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ 2007 से शुरु हुए आन्दोलनों से इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की जा सकती है कि किस तरह झूठे आरोप, झूठी घटना, झूठी पुलिस, सरकार की वायदाखिलाफी और लोकतांत्रिक ढांचे की लंबी न्याय प्रक्रिया ने इस पूरे समुदाय को बेजुबान बनाने का हर संभव प्रयास किया.
पर बाटला हाउस एनकाउंटर मुस्लिम केंद्रित राजनीति का वो प्रस्थान बिंदु था जब मुस्लिम बाबरी विध्वंस की उस पुरानी सांप्रदायिक राजनीति से अपने को ठगा महसूस करते हुए अपने ऊपर आतंकवाद के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ लामबंद होते हुए हिंदुस्तान की राजनीति में नए अध्याय का शुरुआत करने लगा. जो सत्ताधारी पार्टियों के भविष्य के लिए शुभ संकेत न था और वे फिर से उसे पुराने ढर्रे पर लाने को बेचैन थीं.
आज जो सपा सरकार बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को छोड़ने की बात कह रही है, उसी के समर्थन वाली केन्द्र सरकार के दौर में बाटला हाउस फर्जी एनकाउंटर हुआ. दरअसल सपा की कोई नीति नहीं है और यह एक फासिस्ट एजेंडे के तहत कार्य कर रही है नहीं तो यही उस वक्त मानवता विरोधी परमाणु समझौता के जहां पक्ष में बिकी वहीं आज यह एनसीटीसी के पक्ष में है. एनसीटीसी आईबी के अधीन कार्य करेगी. वो आईबी जिसने पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि आतंकवादी के रूप में स्थापित कर आज पूरी राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है. दूसरे आज जो पूरा आतंकवाद का वैश्विक विचार है यह उसकी वाहक है.
बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के मामले में भावुकता से ज्यादा संजीदगी से पूरी इस आतंक की राजनीति पर बात करनी होगी. लेकिन एक बात है कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के उत्पीड़न के इस आंदोलन ने इसे राजनीति के केन्द्र में ला दिया है कि आतंकावाद कानून-व्यवस्था से जुड़ा सवाल न होकर राजनीतिक सवाल है तभी तो सरकार बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को छोड़ने की बात कह रही है. पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन संस्थाओं का भी सवाल है जो इसी राज्य व्यवस्था का ढांचा हैं. चाहे वो पुलिस हो या फिर न्यायपालिका. तत्कालीन पुलिस प्रमुख विक्रम सिंह और एडीजी बृजलाल ने जिस योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम नौजवानों को आतंकी घटनाओं में निरुद्ध किया या फिर यूपी एसटीएफ या पुलिस के वो अधिकारी जिन्होंने आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को लंबे समय तक जेलों में सड़ाने का प्रारुप तैयार किया, उनकी व्यवस्था के सांस्थानिक ढांचे में रहते हुए यह कैसा न्याय? या फिर फैजाबाद न्यायालय के न्यायाधीश आर के गौतम जो इस बात को कहते हों कि हमें इन लड़कों को फांसी पर चढ़ना है, ऐसे तत्वों के रहते हुए कैसा न्याय?
दरअसल ‘होम ग्रॉन टेररिज्म’ की पूरी व्याख्या में राज्य बार-बार अपनी नाकामियों को छुपाते हुए एक ऐसे फासिस्ट तंत्र की रचना कर रहा है जहां आतंकवाद न्याय न मिलने के असंतोष की प्रक्रिया से पैदा होता दिखाई दे. जैसे कभी कहा जाता है कि अमुक घटना बाबरी ढांचे से आहत होकर की गई या फिर गुजरात 2002 के दंगों से आहत होकर. पर इसके मूल में इस पूरे समुदाय पर आतंकवाद का मुल्लमा चढ़ाना ही अंतिम लक्ष्य होता है. आज राजनीति के केंद्र बिंदु में आतंकी घटनाओं के जांच की बात क्यों नहीं आ रही है? जबकि कचहरी धमाकों के बाद 24 दिसंबर को एडीजी बृजलाल ने कहा था कि कचहरियों में हुए धमाकों की मॉडस ऑपरेंडि मक्का मस्जिद और गोकुल चाट भंडार पर हुई घटना से मेल खाती है जिसकी सच्चाई भी अब सबके सामने आ गई है कि इन घटनाओं को हिन्दुत्वादी तत्वों ने अंजाम दिया था.
यहां एक बात महत्वपूर्ण है कि फैजाबाद कचहरी में हुए धमाके भाजपा अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह और उपाध्यक्ष महेश पांडे के बिस्तर पर हुआ और दोनों वहां से चंपत थे. इस घटना में आम नागरिक मारे गए. वहीं 31 दिसंबर 2007 की रात में नशे में धुत सीआरपीएफ रामपुर के जवानों ने आपस में ही गोलीबारी की जिसे रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर आंतकी घटना के रूप में प्रचारित किया गया. यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2008 में कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता बम बनाते हुए मकान सहित उड़ गए जिस पर श्रीप्रकाश जायसवाल ने जब कहा कि सीबीआई जांच करवाई जाए तो मायावती ने कहा कि आगे कचहरी धमाकों और सीआरपीएफ कैंप पर हमले की जांच करवा ली जाए. और मामला ठंडे बस्ते में चला गया.
आज अगर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के न्याय का सवाल उठ रहा है तो वह इन घटनाओं की जांच के बिना अधूरा रह जाएगा. दरअसल इस पूरे दबाव की शुरुआत 23 नवंबर 2007 के कचहरी धमाकों के बाद 12 दिसंबर को आजमगढ़ से तारिक कासमी और 16 दिसंबर को मडि़याहूं, जौनपुर से खालिद मुजाहिद को एसटीएफ द्वारा उठाए जाने के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के रूप में हुई. जहां तारिक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना रानी की सराय में 14 दिसंबर को उनके दादा अजहर अली द्वारा दर्ज करायी गई. तो वहीं 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश एसटीफ द्वारा मडि़याहूं, जौनपुर से उठाए गए खालिद की पुष्टि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अघिकारी क्षेत्राधिकारी मडि़याहूं ने लिखित रूप में की है. जो यूपी एसटीएफ की उस पूरी थ्योरी को ही बेनकाब करती है कि इन दोनों की गिरफ्तारी आरडीएक्स, डेटोनेटर के साथ 22 दिसंबर 2007 की सुबह बाराबंकी रेलवे स्टेशन से की गई थी.
दरअसल आजमगढ़ में गिरफ्तारी के खिलाफ जबर्दस्त आंदोलन, बंद और घेराव शुरू हो गया था और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के चौधरी चंद्रपाल सिंह ने प्रशासन को यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर 21 दिसंबर को तारिक-खालिद के बारे में नहीं बताया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे. इस दबाव में आजमगढ़ के स्थानीय समाचार पत्रों में पुलिस ने यह भी कहा कि हम इन्हें खोजने के लिए विशेष जांच टीम गठित कर चुके हैं. दूसरा तथ्य, एसटीएफ का कहना है कि आरडीएक्स और डेटोनेटर बरामदगी के साथ दोनों नौजवानों के मोबाइल 22 दिसंबर 2007 की सुबह 9 बजे तक स्विच ऑफ कर दिए गए. पर एसटीएफ के विवेचना अधिकारी ने जो कॉल डिटेल दाखिल की उसमें खालिद मुजाहिद के पास बरामद मोबाइल नंबर पर दिनांक 22 दिसंबर 2007 को दिन में 11 बजकर 49 मिनट पर एसएसएस आया है जो एसटीएफ की बात को ही खारिज करता है.
राज्य इस बात को स्थापित करने की कोशिश में रहा कि हमारे गांव-छोटे कस्बों में समाज और देश के खिलाफ युद्व करने वाले मुस्लिम जेहादियों का बोलबाला बढ़ रहा है. इसका खामियाजा उन मुस्लिम बहुल इलाकों को झेलना पड़ा जहां वो दिखते थे पर राजकीय दमन के रूप में. प्रतिरोध का निरंतर विकास होता रहा. इस परिघटना से राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़े मुस्लिम समुदाय जिसके साथ सांप्रदायिक दंगों के वक्त सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दल आ जाते थे वे आतंकवाद के नाम पर किनारा कस लिए. हिंदुस्तानी राजनीति में आतंकवाद के नाम पर सचमुच यह नया प्रयोग था. सपा जैसे राजनीतिक दल शुरुआत में इन स्थितियों को भांप नहीं पाए और जब भांपे तब तक मुस्लिमों में यह भावना प्रबल हो गयी कि इस आफत में उनके साथ कोई नहीं है.
आतंकवाद के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिवाद करने का श्रेय नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी को जाता है. एमवाई समीकरण पर आधारित सपा ने ऐसे में अबू आसिम आजमी जैसे अपने विवादास्पद मुस्लिम चेहरे को आगे लाकर पारी शुरू की पर बात नहीं बन पायी. सपा शायद इस बदली हुई परिस्थिति का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आकलन नहीं कर पायी. मसलन अगर आजमगढ़ में ही देखें तो पूरा बेल्ट एक दौर में मंडल के बाद उभरे अस्मितावादी ‘संस्कृतिकरण’ की राजनीति का गढ़ रहा है और उस दौर में सांप्रदायिक राजनीति को यहां के पिछड़े-दलित तबके ने इस नारे के साथ खारिज कर दिया ‘मिले मुलायम-कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम.’ लेकिन आज हम साफ देख सकते हैं कि आतंकवाद के बहाने यहीं पर इन्हीं जातियों का एक बड़ा तबका वो सारे नारे लगा रहा था जिसे उसने 92 में खारिज कर दिया था.
दरअसल आज आजमगढ़ में हिन्दुत्वादी राजनीति के लिए उसके इतिहास में सबसे बेहतर मौका है. मसलन 90 में यह गिरोह जहां काग्रेस, बसपा, सपा, वामपंथियों और जनता दल जैसी पार्टियों पर उनके मुस्लिमपरस्त होने की लानत देकर हिंदुओं को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था जिसमें उनको इसलिए सफलता नहीं मिल पा रही थी क्योंकि पिछड़ी-दलित जातियों का संस्कृतिकरण अस्मितावादी चेहरे के साथ ही चल रहा था जिसमें उसकी राजनैतिक जरूरत अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़कर रखना था. लेकिन आज मंडल की उपज इन जातियों की राजनीति का सांस्कृतिक तौर पर पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण हो चुका है. जिसके चलते एक ओर जहां वे संघ परिवार से अपने फर्क को खत्म करके उसी की कतार में खड़े दिखने लगे वहीं मुस्लिमों में भी ये विचार मजबूत होने लगा कि इन पार्टियों और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह गया और अब हमें भाजपा के डर से मुक्त होकर अपनी राजनीतिक गोलबंदी करनी चाहिए. जिसकी परिणति बाटला हाउस के बाद सतह पर आई राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल में हुई. ये ऐसी स्थिति है जो हिन्दुत्वादियों को आजमगढ़ में पनपने के लिए 90 के उस दौर से भी ज्यादा स्पेस देती है. हिन्दुत्वादी, उलेमा काउंसिल की परछाई को उसके शरीर से भी बड़ा स्थापित कर अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हैं.
मुस्लिम केंद्रित राजनीति को आजादी के बाद से ही फतवा आधारित राजनिति तक सीमित करने की कोशिश सत्ताधारी पार्टियों ने की. मुस्लिमों को एक दोषी और पीड़ित समाज के बतौर ही देखा गया. और इस अपराध बोध को मुस्लिमों के भीतर पनपाया गया कि आप दोषी हैं फिर भी हम आपका साथ दे रहे हैं. इस राजनीतिक शतरंज की बिसात को फैलाने का एक और मौका 2008 में आजमगढ़ में हुए उप-चुनावों में बसपा को मिला. बसपा सरकार ने तारिक और खालिद की गिरफ्तारी को लेकर आरडी निमेष जांच आयोग का गठन करके छह महीने में रिपोर्ट पेश करने का वादा किया. इस चुनाव में बसपा के अकबर अममद डम्पी ने भाजपा के रमाकान्त यादव को 54251 वोटों से हराया और सपा तीसरे नम्बर पर रही. यह पहला चुनाव था जब सपा के ‘एमवाई’ समीकरण के टूटने और इस क्षेत्र को गुजरात बना देने के नारे गूंजने लगे. ‘हिन्दुत्व के आगे नहीं चला मुलायम का एमवाई नारा’ 17 अप्रैल, 2008 हिन्दुस्तान.
बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को छोड़ने की सपा की कवायद को समझने के लिए उस दौर में बटला हाउस के बाद बनी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी राजनीतिक पार्टियों के बनने की परिघटना को भी समझना होगा. क्योंकि मुस्लिम युवाओं में अलग पार्टी बनाने की जिस भावना को देखा गया उसने इस खास समय में इसलिए उफान मारा क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि उनकी खोज-खबर लेने वाला कोई नहीं है. इस सोच को रखने वाला यह तबका 2002 के बाद की राजनीतिक स्थितियों की पैदाइस था जबकि 92 के दौर को देखने वाला तबका अलग पार्टी बनाने की वकालत नहीं कर रहा था. 2009 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का सत्ता के परिदृश्य से बाहर रहने के कारण भी यह प्रयोग हो सका क्योंकि कोई डर नहीं था.
मुस्लिम समाज में उभरा यह राजनीतिक समीकरण मजबूर करके सरकार में भागीदारी चाहता है. इसे हम यूपी के तराई क्षेत्रों में सक्रिय पीस पार्टी के नारे में भी देख सकते हैं ‘मजबूर नहीं मजबूत बनो’. जो मुस्लिम राजनीति हराने-जिताने तक सीमित थी उसमें बदला लेने की भावना इस नयी राजनीति ने सम्प्रेषित किया. यह बदला उसके अपनों से खास तौर पर सपा जैसी राजनीतिक पार्टियों से था जिन्होंने यह कह कर सालों-साल से वोट लिया था कि हम आपको बचाएंगे. हर घटना के बाद सफाई देने की जगह इसने प्रतिरोध से जवाब देने की कोशिश की. वजूद और हुकूक तक सीमित राजनीति छीनने की बात करने लगी. इसे हम बाटला हाउस के मुद्दे पर उलेमा काउंसिल द्वारा दिल्ली-लखनउ की रैलियों में आसानी से देख सकते हैं. राजनीति की कमान मौलानाओं के हाथ में और धुरी युवा. यह समीकरण इसलिए भी कारगर हुआ क्योंकि राजनीति के केंद्र में वह युवा था जिसने अपनों को गोलियों से छलनी और सालों-साल के लिए नरक से भी बुरी जेलों में ठूंसे जाते देखा था. और उसमें यह डर भी था कि उसका नंबर कब आ जाए और उसे पूरा विश्वास था कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा और ऐसे में अलग पार्टी बनाने की भावना उसमें प्रबल हो गयी. जिसमें सबक सिखाने की भावना के साथ यह निहित था कि जो सफलता मिलेगी वह उसका बोनस होगा.
आजमगढ़ में 2009 के लोकसभा चुनावों में जहां अकबर अहमद डम्पी जैसे मुस्लिम राजनीतिक चेहरे को भी हार का मुंह देखना पड़ा और ऐसा मुस्लिम समाज ने यह जानते हुए किया कि इससे भाजपा जीत जाएगी. क्योंकि बसपा ने उप-चुनावों के वक्त कचहरी धमाकों के आरोपी तारिक कासमी और खालिद की गिरफ्तारी पर आरडी निमेष जांच का गठन किया जिसे डम्पी के जीतने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. मुस्लिम समाज में यह भावना प्रबल हो गयी की भाजपा ही सत्ता में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम से कम दुश्मन नकाब में तो नहीं रहेगा. मुस्लिम समाज ने सांप्रदायिक परिकल्पना, सांप्रदायिक तर्कों और सांप्रदायिक उत्तरों में इस बात को अब समझ लिया था कि उसके लिए यह कितना झूठ और छद्म है. इस भावना को काले झंडों के साए में दिग्विजय सिंह की यात्रा के वक्त आजमगढ़ की सड़कों पर लहराते तख्तियों में आसानी से देख सकते हैं ‘नए जाल लाए हैं, पुराने शिकारी आए हैं’.
इसी दौर में हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की आतंकी घटनाओं में संलिप्तता ने मुस्लिम राजनीति में एक प्रतिरोध को जन्म दिया. और इसमें हिंदुत्ववादियों के खिलाफ जो आग थी उसमें एक खास तरह की सांप्रदायिकता निहित थी. क्योंकि एक सांप्रदायिकता के खिलाफ जब उसी भाषा में प्रतिक्रिया की जाती है तो नतीजे के तौर में सांप्रदायिकता ही मजबूत होती है.
ऐसा स्वतःस्फूर्त नहीं हुआ. यह कांग्रेस की प्रायोजित चाल थी कि किस तरह से भाजपा को मुद्दा विहीन कर दिया जाय और दोषी और पीड़ित के अंतर्द्वंद से गुजर रहे मुस्लिमों का वोट भी हथिया लिया जाय. क्योंकि इससे पहले नांदेड़ और परभनी में भी हिंदुत्ववादियों का नाम आ चुका था. और दिग्विजय सिंह यह बात हर बार दुहराते हैं कि उनके पास बजरंग दल और संघ परिवार के आतंकी घटनाओं में लिप्त होने के सुबूत हैं. पर कांग्रेस ने कभी भी संघ परिवार या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को कोई प्रयास नहीं किया. हमारे जमीन के आतंकवादी के नाम पर आतंकवाद की राजनीति का खेल खेलने वाली कांग्रेस को इस बात की तनिक भी संभावना नहीं थी कि इससे नए तरह की राजनीति का उदय हो सकता है.
कांग्रेस को अपनी जड़ें यूपी में मजबूत करने में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी बाधा थी जो सपा से होते हुए 2007 के विधानसभा चुनावों में बसपा की झोली में चला गया था. यूपी में तकरीबन 18 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम वोटर 160 विधानसभा सीटों पर हार-जीत का फैसला करते हैं. 25 जिलों में मुस्लिमों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है. इसी रणनीति के तहत 2007 के विधानसभा चुनावों को मायावती ने लड़ा जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक बसपा के पास थे. नयी पार्टियों के बनने से अब मुस्लिम वोट बिखर चुका है. यूपी के तराई क्षेत्र में पीस पार्टी ने खामोशी से योगी की सांप्रदायिकता के खिलाफ अंसारी जातियों को एकजुट किया. 2009 लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी में कांग्रेस को मिला ‘जनादेश’ भी कुछ हद तक इसी समीकरण का नतीजा था. क्योंकि पीस पार्टी के लड़ने की वजह से मुस्लिम वोट बैंक सपा-बसपा से कटा जिसका फायदा कांग्रेस को मिला अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस को मिला जनादेश का असर सिर्फ तराई तक ही सीमित क्यों रहता?
इन राजनीतिक परिस्थितियों और संभावित मुस्लिम केंद्रित राजनीतिक दलों के उभरने से यूपी में एक खास तरह का राजनीतिक समीकरण बनने की प्रबल संभावना में सपा ने इस बात को भांप लिया कि अगर आतंकवाद के उत्पीड़न के नाम पर राजनीतिक दल बन सकते हैं तो हम क्यों न उनके पॉपुलर एजेंडे को अपना एजेंडा बना लें. ऐसा कर वह दो स्तरों पर अपने मंसूबे में खुद को कामयाब होती देख रही है. एक तो वह कांग्रेस के हौव्वे को हवा बना देना चाहती है दूसरा उसके केन्द्र में मुस्लिम केन्द्रित राजनीतिक दल हैं. क्योंकि इस चुनाव में पीस पार्टी ने जहां 4 सीटें निकाली और 10 सीटों पर 25 से 30 हजार वोट पाया तो वहीं कौमी एकता दल के अंसारी बंधु राजभर-चौहान जैसी पिछड़ी जातियों की राजनीतिक पार्टियों के बल पर अपने दबदबे को बरकरार रखे हुए हैं. दूसरे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसे राजनीतिक दल सीपीएम व जन संघर्ष मोर्चा जैसे वाम जनाधार वाले दलों के साथ खडे़ दिख रहे हैं. आज लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सभी आतंकवादी घटनाओं की समयबद्ध न्यायिक जांच करवाना ही एक मात्र विकल्प है.